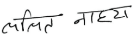खरतरगच्छ का उद्भव
खरतरगच्छाचार्य श्री जिनपीयूषसागरसूरि
इतिहास विश्व का दर्पण है। जिसका जैसा बिम्ब होगा उसमें वैसा ही प्रतिबिम्बित होगा। खरतरगच्छ का आदिकाल विक्रम की ग्यारहवीं सदी से तेरहवीं सदी का है। खरतरगच्छ का बीजारोपण, सिंचन एवं अंकुरण इसी काल में हुआ। पश्चकाल में खरतरगच्छ रूप सुविहित मार्ग/विधि पक्ष का विकास के चरम शिखर पर आरोहण हुआ। महामहिम कान्तदर्शी आचार्य जिनेश्वरसूरि खरतरगच्छ की आधारशिला हैं। यही वह बीज है जिससे खरतरगच्छ का वटवृक्ष अंकुरित एवं पल्लवित हुआ। जिस गच्छ में जिन संस्कृति को ज्योर्तिमय बनाने के लिए समय-समय पर अनेकानेक कार्य एवं बलिदान हुए, उस गच्छ का आचार्य जिनेश्वर सूरि द्वारा प्रवर्तित होना एक स्वर्णिम ऐतिहासिक पहल है। वास्तव में जैसा बीज होगा तदनुरूप ही उसका वृक्ष होगा। आखिर बीज में ही तो आच्छ है विशाल वटवृक्ष का भविष्य। आचार्य जिनेश्वरसूरि के प्रखर पाण्डित्य, उत्कृष्ट चारित्र, गम्भीर व्यक्तिव और प्रबुद्ध कृत्तिव के फलस्वरूप ही उनका गच्छ अनुपमेय व्यवस्थामूलक तथा नैतिक पृष्ठभूमि में प्रतिष्ठित रहा। वे अपने समय के अद्वितीय प्रज्ञा-निष्प व्यक्तिव थे।
चैत्यवासी परम्परा ने जैन संस्कृति की उज्ज्वलता को निर्विवादतः क्षति पहुंचायी। ग्यारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में आचार्य जिनेश्वरसूरि एवं आचार्य बुद्धिसागरसूरि बन्धु युगल ने इस ओर सर्वप्रथम कदम उठाने का साहस किया। दोनों आचार्य चैत्यवासियों को प्रबुद्ध करने की भावना से अणहिलपुरपत्तन पहुंचे। चैत्यवासियों का सर्वाधिकार एवं प्रभाव होने के कारण उन्हें उस नगर में रहने के लिए किसी ने भी स्थान नहीं दिया, कारण वहां के राजमान्य चैत्यवासियों ने सुविहित मुनियों का पत्तन में ठहरना वर्जित करा रखा था। परंतु वहां का राजपुरोहित दोनों आचार्यों की विद्वता तथा प्रतिभा से अत्यन्त प्रभावित हुआ उसने अपनी पाठशाला /अश्वशाला ठहरने के लिए दे दी। जब चैत्यवासियों को वस्तुस्थिति का पता चला, तो उन्होंने दोनों आचार्यों को निकालने हेतु उचित-अनुचित उपाय किये, किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। अन्त में राजपुरोहित की प्रेरणा से महाराजा-दुर्लभराज की सभा में आचार्य जिनेश्वरसूरि और चैत्यवासियों के बीच परस्पर शास्त्रार्थ हुआ। चैत्यवासियों के विरोध में उनके क्रांतिकारी स्वर अभेद्य रहे। उन्हें सर्वप्रथम सफलता मिली चैत्यवासियों के साथ हुए शास्त्रार्थ में। दो पक्ष में एक को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए उस समय शास्त्रार्थ प्रमुख था। जिनेश्वरसूरि अपनी स्फूरणशील मनीषा से चैत्यवासियों को पराभूत करने प्रथम चरण में सफल एवं विजयी सिद्ध हुए।
खरतरगच्छ कब-कहां-किसके द्वारा-किसको
शास्त्रार्थ विजेता जिनेश्वरसूरि को दुर्लभराज ने खरतरविरुद्ध से सम्मानित किया जिसका अर्थ होता है-खरा, स्पष्टवादी, हृदयशील, अतितेजस्वी, शुद्ध । वस्तुतः खरतरगच्छ के नामकरण का सम्बन्ध उसी शास्त्रार्थ विजय से है।
आचार्य जिनेश्वरसूरि का शास्त्रार्थ किस चैत्यवासी आचार्य के साथ हुआ, यह भी उल्लेखनीय है।
वृद्धाचार्य प्रबन्धावली में लिखा है कि आचार्य जिनेश्वरसूरि का चुलसीगच्छ (चौरासी गच्छ) के भट्टारक द्रव्यलिंगी चैत्यवासी के साथ दुर्लभराजा की सभा में वाद हुआ। उसमें चैत्यवासी आचार्य पराजित हुए और जिनेश्वरसूरि विजित (खरतरगच्छ वृहद गुर्वावली, पृष्ठ 90)। उपाध्याय जिनपाल के उल्लेखानुसार शास्त्रार्थ के समय चैत्यवासी परम्परा के चौरासी आचार्य उपस्थित थे, जिनकी अध्यक्षता सूराचार्य ने की युगप्रधानाचार्य गुर्वावली, पृष्ठ 3)।
सूराचार्य व्याकरण, न्याय के विशेषज्ञ एवं शास्त्रार्थ-निपुण थे। उन्होंने राजा भोज की सभा में वाद-विजय कर ख्याति अर्जित की थी। गुर्जर-नरेश भीम भी उनसे प्रभावित हुआ। ये अणहिल्लपुर में ही जन्मे, दीक्षित हुए। एक प्रभावशाली आचार्य होते हुए भी शास्त्रीय मर्यादाओं को विश्रृंखलित कर बैठे और शास्त्रीय आचारमूलक चर्चा में उन्हें पराजित होना पड़ा। प्रभावक चरितकार के अनुसार सूराचार्य ने अपने जीवन की सांध्य–वेला में अनशन संलेखना वृत्त स्वीकार किया थाप्रभावक चरित्र में सूराचार्य का परिचय सूराचार्य-प्रबंध' नाम से 259 पद्यों में प्रस्तुत है।
जिनेश्वर एवं सूर के मध्य जो शास्त्रार्थ हुआ, उसका उपाध्याय जिनपाल ने इस प्रकार वर्णन किया है-
आचार्य वर्द्धमानसूरि एवं जिनेश्वरसूरि (अन्य प्रमाणों के अनुसार आचार्य जिनेश्वरसूरि एवं आचार्य बुद्धिसागरसूरि) राजसभा में शास्त्रार्थ करने के लिए पहुंचे। यहाँ उन्होंने राजा द्वारा निवेदित स्थान पर प्रमार्जन करके आसन ग्रहण किया। राजा चैत्यवासियों की तरह उन्हें भी सम्मानार्थ ताम्बूल (पान) भेंट करने लगेयह देखकर जिनेश्वरसूरि ने कहा राजन्! साधु पुरुषों को ताम्बूल का सेवन अनुचित है, क्योंकि शास्त्रों में कहा है-
ब्रह्मचारियतीनां च विधवानां च योषिताम् ।
ताम्बूल भक्षणं विप्रा! गोमांस विशिष्यते ।।
अर्थात् ब्रह्मचारी, यति एवं विधवाओं को ताम्बूल भक्षण करना गोमांस के समान है।
यह सुनकर वहाँ उपस्थित विवेकवान् जैन संघ की आचार्य के प्रति बड़ी श्रद्धा उत्प हुई।
र के समय वर्द्धमानसूरि ने कहा कि हमारी ओर से पण्डित जिनेश्वरसूरि उत्तर प्रत्युत्तर करेंगे और ये जो कहेंगे, वह हमें मान्य होगा। यह सुनकर सभी ने कहा कि यह उचित है। इसके बाद पूर्व पक्ष ग्रहण करते हुए सूराचार्य ने कहा- जो मुनि वसति में निवास करते हैं, वे प्रायः षड्दर्शन से बाहर हैं। प्रदर्शनों में श्रवणक जटी आदि का समावेश है, किन्तु ये लोग इनमें से कोई भी नहीं हैं। अपने तथ्य की प्रामाणिक पुष्टि के लिए उन्होंने नूतन ‘वादस्थल' नामक ग्रन्थ प्रस्तुत किया। जिनेश्वरसूरि ने ‘भावी का अतीत की तरह उपचार होता है- इस न्याय का अवलम्बन लेकर कहा- नृपेन्द्र दुर्लभराज! आपके राज्य में पूर्व पुरुषों द्वारा निर्धारित नीति चलती है या वर्तमान पुरुषों द्वारा निर्मापित नवीन नीति?
राजा ने कहा- 'पूर्व पुरुषों की बनाई नीति ही हमारे देश में प्रचलित है, नवीन राजनीति नहीं। और चतुर्दश पूर्वधर आदि द्वारा निर्दिष्ट मार्ग ही प्रमाण स्वरूप माना जाता है, दूसरा नहीं। राजन्! हम लोग बहुत दूर देश से आये हैं, अतः हमारे पूर्वाचार्यों द्वारा रचित सिद्धांत-ग्रन्थ हम अपने साथ नहीं लाये हैं।
इसलिए इन चैत्यवासी आचार्यों के मठों से हमारे पूर्वाचार्यों द्वारा विरचित सिद्धांत ग्रन्थों को मंगवा दीजिये, ताकि उनके आधार पर मार्ग–अमार्ग/सत्य-असत्य का निर्णय किया जा सके। तब राजा ने उन चैत्यवासी यतियों को सम्बोधित करके कहा- ये वसतिवासी मुनि ठीक कहते हैं। पुस्तकें लाने मैं अपने राजकीय कर्मचारी पुरुषों को भेजता हूँ। आप अपने यहां सन्देश भेज दें, जिससे उन्हें वे पुस्तकें सौंप दी जायें। चैत्यवासी यति यह जान गए थे कि हमारा पक्ष दुर्बल रहेगा और इनका पक्ष प्रबल, अतः उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया और चुपचाप रहे। तब राजा ने ही राजकीय पुरुषों को सिद्धांत ग्रन्थों का वेष्टन/गठरी लाने को भेजा। वे गए और शीघ्र ही ग्रन्थ ले आए। ग्रन्थों की गठरी खोलने पर सर्वप्रथम वह पृष्ठ दिखाई दिया, जिसमें निम्नलिखित गाथा प्रथम थी-
अनट्ठं पगडलेणं, वइज्जसयणसणं।
उच्चार—भूमि-संप , इत्थीपसुविवज्जियं ।।।
अर्थात् साधु को ऐसे स्थान में ठहरना चाहिए जो साधु के निमित्त नहीं, किन्तु अन्य किसी के लिए बनाया गया हो, जिसमें खान-पान और सोने की सुविधा हो, जिसमें मल-मूत्र त्याग के लिए उपयुक्त स्थान निश्चित हो और जो स्त्री, पशु, नपुंसक आदि से वर्जित हो।
इस प्रकार ‘वसति (वस्ती) में साधुओं को रहना चाहिए, न कि देव मंदिरों में यह सुनकर राजा ने कहा- यह तो ठीक ही कहा है। सारे अधिकारियों ने जान लिया कि हमारे चैत्यवासी गुरू निरुत्तर हो गये हैं। तब वहाँ पर उपस्थित सारे अधिकारीगण एवं मंत्री श्रीकरण राजा से प्रार्थना करने लगे- ये चैत्यवासी साधु तो हमारे गुरू हैं। इन लोगों ने समझा था कि राजा हमें बहुत मानते है। इसलिए हमारे संकोच से साधुओं के प्रति भी वे पक्षपात करेंगे ही। परन्तु राजा निष्पक्ष और न्यायप्रिय था। यह देखकर जिनेश्वरसूरि ने कहा- महाराज! यहाँ कोई मंत्री श्रीकरण का गुरू है, तो कोई पश्वों का गुरू है। अधिक क्या कहें, इनमें सभी परस्पर गुरू-शिष्य का सम्बन्ध बना हुआ है। हम आपसे पूछते हैं कि इस लाठी का सम्बन्ध किसके साथ है? राजा ने कहा- इसका सम्बन्ध मेरे साथ है। जिनेश्वरसूरि ने कहा- महाराज! इस तरह सब कोई किसी न किसी का सम्बन्धी बना हुआ है, किन्तु मेरा कोई सम्बन्धी नहीं है। यह सुनकर राजा बोला- आप मेरे आत्म-सम्बन्धी गुरू हैं।
अचानक राजा ने अपने अधिकारियों से कहा- अरे! अन्य सभी आचार्यों के लिए रत्नपट्ट्ट से निर्मित सात गदिका/गद्दियां बैठने के लिए हैं और ये चरित्रशील गुरू नीचे सामान्य आसन पर बैठे हैं, क्या हमारे यहाँ तदनुकूल गादियाँ नहीं? इनके लिए भी विशिष्ठ गदिदका लाओ। यह सुनकर आचार्य जिनेश्वरसूरि ने कहा- राजन्! साधुओं को गद्दिका पर बैठना उचित नहीं है।
शास्त्रों में कहा है-
भवति नियत मेवा संयमः स्याद्-विभूषा, नृपति ककुद । एतल्लोक हासश्व भिजोः ।
स्फुटतर इह संगः सातशीलत्वमुच्चै शितिन खलु मुमुक्षोः संगतं गदिकादि।।
अर्थात् मुमुक्षु को गादी आदि का उपयोग करना योग्य नहीं है। यह तो श्रृंगार और शरीर-सुख का एक साधन है, जिससे असंयमित मन अवश्य चंचल हो जाता है। इससे लोक में साधु की हँसी होती है। यह स्पष्टतया आसक्तिकारक है और इससे अत्यंत शारीरिक सुखशीलता बढ़ती है। इसलिए हे राजन् !
इसकी हमें आवश्यकता नहीं है।
ये पंक्तियाँ सुन राजा उनके प्रति श्रद्धाभिभूत हो गया और उसने पूछा- "आप कहाँ निवास करते हैं। जिनेश्वरसूरि ने कहा- महाराज! जिस नगर में अनेक विपक्षी हों, वहाँ स्थान की प्राप्ति कैसी? उनका यह उत्तर सुनकर राजा ने कहा- नगर के ‘कर डिहटी (प्रभावक चरित के अनुसार व्रीहिहट्टी) नामक मोहल्ले में एक वंशहीन पुरुष का विशाल भवन खाली पड़ा है, उसमें आप निवास करें। राजा की आज्ञा से उसी क्षण वह स्थान प्राप्त हो गया। राजा ने पूछा- आपके भोजन की क्या व्यवस्था है? सूरि ने उत्तर दिया महाराज! भोजन की भी वैसी कठिनता है। राजा ने पूछा- आप कितने साधु हैं? जिनेश्वरसूरि ने कहा- अठारह साधु हैं। तब राजा ने कहा कि इसकी व्यवस्था हो जाएगीआप राजपिण्ड का सेवन करेंतब जिनेश्वरसूरि ने कहा- महाराज! साधुओं को राजपिण्ड कल्प्य नहीं है। राजपिण्ड का सेवन शास्त्र में निषिद्ध है। राजा बोला- अस्तु! ऐसा न सही। भिक्षा के समय राजकर्मचारी के साथ रहने से आपलोगों की भिक्षा सुलभ हो जाएगी। ... इस प्रकार वाद-विवाद में विपक्षियों को परास्त करके अन्त में राजा और राजकीय अधिकारी पुरूषों के साथ वर्धमानसूरि, जिनेश्वरसूरि आदि ने सर्वप्रथम गुजरात में वसति में प्रवेश किया और सर्वप्रथम गुजरात में वसति–मार्ग (युगप्रधानाचार्य-गुर्वावली, पृष्ठ 3) की स्थापना हुई।"
उक्त उल्लेखों से स्पष्ट है कि आचार्य जिनेश्वर ने सूराचार्य एवं राजा की सभी युक्तियों का बड़ी कुशलतापूर्वक खण्डन करते हुए यथार्थता का निरूपण किया। जिनेश्वरसूरि ने चैत्यवासियों का जीवन कलुषित एवं अत्यन्त अपवादपर्ण बताया। जिनेश्वरसरि के वाकचातुर्य के कारण तथा प्रखर पाण्डित्य से न केवल उनके विपक्षी ही पराजित हुए अपितु तत्रस्थ आसीन विद्वान एवं गणमान्य लोग भी प्रभावित हुए थे। जिनेश्वरसूरि की स्पष्टवादिता, आचार-निष्ठा तथा प्रखर तेजस्विता को देखकर ही उन्हें “खरतर' विरुद प्रदान किया अथवा “खरतर सम्बोधन से सम्बोधित किया गया।
खरतर नामकरण
‘खरतर' शब्द प्रखरता का परिचायक है। खरतरगच्छ 'यथा नाम तथा गुण' की उक्ति को चरितार्थ करता है। जिस प्रकार ईसाई समाज में ‘प्यूरीटन' नाम की उत्पत्ति उग्र सुधारवाद के वातावरण को लेकर हुई, उसी प्रकार ‘खरतरगच्छ' के नामकरण का आधार है। 'खरतर' शब्द-सम्बोधन महाराज दुर्लभराज ने आचार्य जिनेश्वरसूरि के लिए किया था। जिनेश्वर वज्रशाखा के अनुगामी थे। उन्होंने चैत्यवासियों को जिस भूमिका पर परास्त किया, इससे उनकी सारे समाज में यशोगाथा फैली। दुर्लभराज ने सभी सभासदों के बीच जिनेश्वर की प्रतिभा का गुणगान किया और उन्हें खरतर/प्रखर बताया। अतः जिनेश्वरसूरि का अनुयायी-वर्ग या प्रभावित वर्ग उनके लिए खरतर सम्बोधन व्यवहृत करने लगाजिनेश्वरसूरि का प्रभाव विस्तृत रूप से फैला। उनका अनुयायी-वर्ग विशाल हो गया। अतः उनकी परम्परा के लिए 'खरतरगच्छ शब्द का उपयोग होने लगा। खरतर–विरुद प्राप्ति का उल्लेख हमें अनेक ऐतिहासिक ग्रन्थों में मिलता है। आचार्य जिनदत्तसूरि ने “तुम्हइहु पहु चाहिल दसिउ हियइ बहुत्तु खरउ विमसउ” इस खरतरगच्छ-सूचक पंक्ति का उल्लेख किया है। इसी तथ्य के सम्बन्ध में पण्डित लालचन्द भगवान दास गांधी ने लिखा है कि- उपर्युक्तमेव गाथायां बहुतु खरउ पदं प्रयुज्य ग्रन्थकर्ताः निजाभिमतस्य विधि पथस्य 'खरतर' इति गच्छ संज्ञा ध्वनितां वितर्व्यते। विधि पथस्यैव तस्य कालक्रमेण प्रचालिता ‘खरतरगच्छ' इत्यभिधायवधि विद्यते। (अपभ्रंश कावयत्रयी, भूमिका, पृष्ठ 116)
वृद्धाचार्य प्रबन्धावलीकार ने स्पष्टतः यह लिखा है कि दुर्लभराज ने परितुष्ट होकर जिनेश्वरसूरि को ‘खरतर विरूद दिया-र । तुट्ठेण खरतर इह विरूदं दि । तओं परं खरतरगच्छो जाओ (वृद्धाचार्य प्रबन्धावली, जिनेश्वरसूरि प्रबन्ध)। यह संदर्भ खरतरगच्छ के लिए एक ऐतिहासिक मूल्य लिए है। खरतर–विरूद की प्राप्ति के बाद खरतरगच्छ उत्प हुआ।
सुमति गणि ने सं. 1295 में गणधर सार्द्ध शतक वृहद वृत्ति में खरतर विरूद प्राप्ति विषयक वर्णन निम्न प्रकार से किया है-
कि बहुनेत्यं वादं कृत्वा विपक्षा िर्णित्य राजामात्य श्रेष्ठि सार्थवाह प्रभृति पुर–प्रधानः पुरूषैः सह भट्टचट्टेषु वसति मार्ग प्रकाशन यशः पताकायमान काव्य बन्धान् दुर्जन जन कर्णशूलान् साटोपं पठत्सु सत्सु प्रविष्टा वसतो प्राप्त खरतर विरूद भगवन्तः श्री जिनेश्वरसूरयः एवं गुर्जरय देशे श्री जिनेश्वरसूरिणा प्रथम चक्रे ।
(गणधर सार्द्ध शतकान्तर्गत प्रकरण, पृष्ठ 11)
आचार्य जिनचन्द्रसूरि का उल्लेख भी यहाँ वर्णनीय है:-
यैः पूज्यैरणहिल्लपत्तनपुरे द्योसिदि शून्य क्षमा वर्षे दुर्लभ राजषर्वादि पराजित्य प्रमाणोक्तिभिः । सरीन चैत्यवासिनः खरतर ख्याति जनेश्चार्पित श्रीमत् सूरिजिनेश्वराः समभवत्तत्पट्ट शोभकराः ।।
(खरतरगच्छ पट्ट्टावली, लेखन काल सं. 1830)
अभिधान राजेन्द्र-कोश में संकलित सन्दर्भ के अनुसार-वैक्रम संवत् 1080 श्रीपत्तने वादिनो जित्वा खरतरेत्याख्यं विरूदं प्राप्तेन जिनेश्वरसूरिणा प्रवर्तिते गच्छे-आत्मप्रबोध (141) आसीत त्तपादपंकजैकमधुकृत् श्रीवर्धमानाभिधः सूरिस्तस्य जिनेश्वराख्यगणभृज्जातो विनेयोत्तमः । यः प्रापत् शिवसिद्धिपक्ति (संवत 1080) शरद श्री पत्तने वादिनो जित्वा सद्विरूद्धं कृति खरतरेत्याख्यां नृपादेर्मुखात।
| (अष्ट.32,अष्ट.)(अभिधान राजेन्द्र-कोश, तृतीय भाग, पृष्ठ 726)
एक अन्य पट्टावली के अनुसार- संवत् 1080 दुर्लभराज सभाये 84 मठपतीन् जीत्वा प्राप्त खरतर विरूदः ।
(उद्धृत-युगप्रधान श्री जिनचन्द्रसूरि, भूमिका, पुष्ठ 40)
वृद्धाचार्य प्रबन्धावली में जिनेश्वरसूरि प्रबंध लिखते हुए खरतरगच्छ की उत्पत्ति एवं शास्त्रार्थ-विजय का काल बताया गया है। उसके अनुसार 'दस सय चउवीसे बच्छरे ते आयरिया मच्छरिणो हारिया।'
(खरतरगच्छ वृहद् गुर्वावली, पृष्ठ 90)
उक्त ‘दस सय चउवीसे' को दस सौ चौवीस की संख्या आंकी गई है। जबकि यह संशोधनीय है।
इसका फलन है-
10x100+4x20=1080
तपागच्छ के आचार्य श्री सोमसुन्दरसूरिजी के शिष्य श्री चारित्ररत्नगणिजी के शिष्य श्री सोमधर्मगणिजी ने विक्रम संवत् अनुमानत 1500 में 'श्री उपदेश सत्तरी नामक ग्रन्थ बनायाउसमें श्री जिनेश्वरसूरिजी से खरतरगच्छ तथा नवांगी वृत्तिकारक श्री अभवदेवसूरिजी खरतरगच्छ में हुए हैं “गच्छः खरतराभिधः" ।
श्री खरतरगच्छ गुर्वावली श्री आचार रत्नाकर के दूसरे प्रकाश के पृष्ठ 104-106 में उल्लेख है (विस्तारभय से संक्षेप विवरण) सुविहित पक्षधारक श्री जिनेश्वरसूरि वीर संवत् 1550 विक्रम संवत् 1080 वीर संवत् 1550 में 'खरतर विरूद्ध प्राप्त किया। तब से कोटिकगच्छ, चन्द्रकुल, वयरीशाखा, खरतरविरूद्ध ऐसा भेद स्थविर साधु, नवीन साधुओं से कहने लगे, यहां से कोटिकगच्छ का नाम खरतरगच्छ प्रसिद्ध हुआ। अतिशयेन खरा सत्य प्रतिज्ञा से ते खरतराः इत्यादि खरतर विरूद्ध को प्राप्त होने वाले श्री जिनेश्वरसरि बडे प्रभावशाली हए हैं।
न्यायवान मध्यस्थ विद्वान ने अंग्रेजी भाषा में सभा समक्ष भाषण देते समय शास्त्रानुसार जैन धर्म के प्राचीन इतिहास संबंधी अनेकों खुलासा किया था, उसमें खरतरगच्छ तपागच्छ की पट्टावली कथन करने में पहले खरतरगच्छ की पट्टावली का कथन किया उसी खरतरगच्छ की पट्टावली में भी श्री जिनेश्वरसूरिजी महाराज से ‘खरतर विरुद्ध लिखा है उसका गुजराती भाषा में अनुवाद सन् 1908 जुलाई माह में ‘सनातन जैन' नामक मासिक पत्र के पृष्ठ 374 से 381 तक में उल्लेख मिलेगा।
युगप्रधान जैन जगत के प्रथम दादागुरूदेव श्री जिनदत्तसूरीश्वरजी कृत 1180 के अनुमान श्री गुरूपारतंत्रय और श्री गणधर सार्द्धशतक आदि प्राचीन ग्रन्थों से भी सिद्ध है।
खरतरगच्छ की स्थापना - स्थापनकर्ता - स्थल सम्बन्धित मिथ्या अभिनिवेश का प्रमाणिक तथ्यों से निराकरण
न्यायभोनिधि श्री आत्मारामजी के प्रबन्ध चिन्तामणि', 'गुर्जरदेश भूपावली,'वनराज चावड़ा प्रबन्ध और फारबस साहब की रची ‘रासमाला' एवं तपा.धर्मसागरजी के प्रवचन परीक्षा आदि पुस्तकों का प्रमाण कर जिनेश्वर सूरि से 'खरतर विरूद्ध और संवत् 1077 में दुर्लभराजा की मृत्यु होने का बतलाकर संवत् 1880 में श्री जिनेश्वरसूरि जी को खरतरविरुद्ध देने का निषेध किया?
महानुभावों ने मायावृत्ति से एकांत हठवाद करके कल्पित अवलम्बनों से जो परिश्रम किया है वह अभिनिवेशिक मिथ्यात्व का कारण ही मालूम होता है। उपर की ऐतिहासिक पुस्तकों में अनेक जगह परस्पर विरुद्धता की बातें बहुत जगह लिखी हुई हैं और एक ही बात में अनेक तरह के मतभेद लिखे हुए हैं। फिर भी देखें 'रासमाला' आदि ऐतिहासिक पुस्तकों में भी श्री दुर्लभराजा ने श्री जिनेश्वरसूरिजी को 'खरतर विरुद्ध दिया ऐसा सिद्ध होता है। देखें-
प्रथम फारबस साहिब की रची ‘रासमाला' नाम की गुजरात के इतिहास की पुस्तक दुसरी आवृत्ति पृष्ठ 105 में -
1. "दुर्लभ राजे राज्य सारी रीते चलाव्यु असुरो ने तेणे बहादुरी थी जीत्या देरां बांध्यां अने घणां धर्मनां काम करयां अणहिल वाडमां तेणे एक दुर्लभ सरोवर बांध्यं श्री जिनेश्वरसूरि पासे ते भणतो हतो तेथी जैनधर्म नो बोध पामी जीवता प्राणियों ऊपर दया करवाना सारा मार्ग मां चालतो' इत्यादि।
2. गुजरात देश का इतिहास मराठी भाषा में मुम्बई निर्णयसागर प्रेस में छपा है जिसमें जिनेश्वरसूरि से 'खरतर विरुद्ध की पुष्टि होती है।
"दुर्लभ राजा ने ही आपले राज्य फार चांगल्या चालविले होते याने देवले वगैरह बांधवून आपल्या राज्यांत प्रष्कल धार्मिक कामें होतीं अन्हिलवाड ये थे दुर्लभ सरोवर नावाचा एक मोठा तलाव आहे, तो याच राजा ने बांधविला असल्याची साक्षव्या सरोवराचे नांव देत आहे। दुर्लभ सेना ने थोडींचीवर्षे राज्य केलें । त्याने आपला गुरूश्री जिनेश्वरसूरिजी म्हणुन होता त्याचे उपदेशा ने जैनधर्माची शिक्षा स्वीकारून त्या धर्मान्त तो मीठा प्रवीण जाला होता त्याने जीव दया उत्तम प्रकारें पालिली' इत्यादि।
उपरोक्त ऐतिहासिक लेख पर भी विवेक बुद्धि से विचार करके देखा जावे तब तो श्री जिनेश्वरसूरिजी को दर्लभ राजा ने खरतर विरुद्ध दिया जिसका निषेध करना कदाग्रह का सूचक व्यर्थ मालूम होता हैक्योंकि जैनधर्म में ऐतिहासिक ग्रन्थों से और श्री जिनेश्वरसूरिजी के चरित्रों से यह तो स्पष्ट मालूम पड़ता है कि अणहिलपुर पाटण में चैत्यवासियों ने राजा से करार करवा लिया था कि हमारे सिवाय अन्य जैनमुनि इस नगरी में रहने न पावे, इसलिए पाटण में शुद्ध संयमियों का आना नहीं होता थाश्री जिनेश्वरसूरि जी इस अनर्थ को तोड़ने के लिए पाटण पधारे। तब चैत्यवासियों ने अपने गुप्तचरों को भेजकर शुद्ध संयमी श्री जिनेश्वरसूरि जी को नगर के बाहर चले जाने का आदेश करवाया। श्री जिनेश्वरसूरि जी ने राजा के निर्णय अनुसार राज्यसभा में चैत्यवासियों से शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित कियादुर्लभ राजा ने श्री जिनेश्वरसूरि जो खरतर विरूद्ध प्रदान किया। तब से पाटण में शुद्ध संयमियों का विचरण चालू हुआ।
निष्पक्षता से विचार करने की बात है कि यदि श्री जिनेश्वरसूरि जी महाराज चैत्यवासियों को पराजित कर शुद्ध संयमी मुनियों का विचरण करवाने का कार्य राजा से नहीं करवाते तो दुर्लभ राजा भक्त होकर श्री जिनेश्वरसूरिजी के पास जैन शास्त्रों का अभ्यास कैसे करता? और जैन धर्मानुरागी होकर विशेष न्यायवान, दयावान, उदातचित्तवाला कैसे बनता? इससे यह प्रमाणित होता है कि यह घटना अवश्य बनी है तभी तो रासमाला और मराठी इतिहास में श्री जिनेश्वरसूरि जी को दुर्लभराजा के गुरू लिखे हैं और राज्यसभा में शास्त्रार्थ होने से विजेताश्री जिनेश्वरसरिजी को दर्लभराजा की तरफ से उनको सत्कार रूप पदवी मिलती है सो यह तो अनेक राजाओं की सभा में अनेक विद्वान जैनाचार्यों ने अनेक विरुद प्राप्त किए हैं जिसके प्रमाण शास्त्र भरे हैं।
अतैव ‘रासमाला व मराठी भाषा के इतिहास से भी दुर्लभ राजा ने श्री जिनेश्वरसूरिजी को खरतर विरूद्ध दिया सिद्ध हो जाता है अन्यथा जहां अणहिलपुर पाटन में शुद्ध संयमियों का जाना और ठहरना नहीं होता था वहां श्री जिनेश्वरसूरिजी के पास राजा के शास्त्राध्ययन करने का और जैनधर्म की शिक्षा पाकर दयावान होना कैसे संभव हो सकता था। सुज्ञ जन स्वयं सत्यार्थ पर विचार करेंगे।
‘प्रबन्ध चिन्तामणि' के नाम से दुर्लभ राजा की मृत्यु वि.सं.1077 में होना बताया है - यह शत-प्रतिशत मिथ्या है क्योंकि 'प्रबन्धचिन्तामणि' में तो 1077 में दुर्लभ राजा के पाटण से काशी की यात्रा जाने का लिखा है कि परंतु मुत्यु होने का संवत् नहीं लिखा, परंतु मुत्यु होने का प्रबन्धचिन्तामणि' के नाम से सं. 1077 में लिखना यह भव्य जीवों को भ्रम में डालकर मृषावाद का संपोषण करना मात्र है।
रासमाला आदि गुजरात के ऐतिहासिक पुस्तकों के आधार से सं.1077 में मृत्यु होने को ठहराने का आग्रह किया वह भी बड़ी भूल है क्योंकि रासमालादि ऐतिहासिक पुस्तक किसी सर्वज्ञ के कथन से कथित नहीं है किन्तु अर्वाचीन जैन व अन्य कथानक इतिहासों के आधार से और चारण भाटादिकों की परम्परागत कथा-कहानियों के आधार से रासमालादि ऐतिहासिक ग्रन्थ लिखे गये हैं, इसलिए इन पुस्तकों की सब बातों पर निश्चय विश्वास करना उचित नहीं है और जो विषय जैनधर्म के ऐतिहासिक आदि अनेक पुस्तकों के प्रमाणानुसार होने से मानना चाहिए और जो बात अभिनिवेशिक मिथ्यात्व का कारण बनता है, जैसे श्री जिनेश्वरसूरिजी को संवत् 1080 में दुर्लभराजा ने 'खरतर विरुद दिया यह प्रमाणिक विषय बहुत शास्त्रों के प्रमाणों से सिद्ध है।
इसलिए चारण भाटादिकों की कथा कहानियां वगैरह के आधार से ‘रासमाला आदि में सं0 1077 में दुर्लभराजा की मृत्यु लिखी उसको प्रमाणिक मान लेना और अनेकानेक शास्त्रानुसार तथा श्री तपागच्छादि के पूर्वाचार्यों की स्वीकृति अनुसार खरतर विरुद का वि.सं. 1080 दुर्लभराजा के द्वारा श्री जिनेश्वरसूरि को प्रदान करने का निषेध करना। यह मात्र गच्छ कदाग्रह एवं अज्ञानता की तुच्छ बुद्धि के सिवाय कुछ नहीं है।
अन्य ऐतिहासिक मतभेद
श्री स्थूलभद्र जी के जन्म, दीक्षा, स्वर्गगमन के वर्षों में चार-चार वर्षों का मतभेद देखा जाता है श्री नवांगी वृत्तिकार श्री अभयदेवसूरि जी के स्वर्गगमन में चार-चार वर्षों का मतभेद देखा जाता है। कलिकाल सर्वज्ञ विरुद धारक श्री हेमचन्द्राचार्य के दीक्षा और आचार्य पद में भी चार-चार वर्षों का मतभेद है। श्री भद्रबाहुस्वामी जी, श्री जिनेश्वरसूरि जी, श्री मल्लवादी सूरि जी तथा धनपाल पण्डित आदि के चरित्रों में भी पाठांतर मतभेद देखा जाता है और इसी तरही तपागच्छ की पट्ट्टावली में भी यावत्श्री हीरविजयसूरि जी को पाटानुसार में कोई कितने पाट पर और कितने पाट पर कोई कितने पाट पर मतांतरों से मानते हैं, इसके लिए 'सम्यक्त्वश्ल्योद्वार आदि में लिखे अनुसार भी सूत्रों पाठान्तर देखा जाता है और भी कितने ही चारित्रादिकों में और ऐतिहासिक बातों में मतभेद पाठान्तर देखने सुनने में आता है, श्री उद्योतनसूरि जी से 84 गच्छ की आपत्ति के सम्बन्ध में भी 3-4 मतान्तर हो गये हैं और ओसवाल, पोरवाल, श्रीमाल, श्रीश्रीमाल आदि जैनी श्रावकों की उत्पति, गौत्र, कुल, स्थापन में भी कितने ही वर्षों का मतभेद देखा जाता है।
ऐसे मत-मतांतरों में कोई हठवादी एकान्त एक बात को पकड़कर मतभेद पाठान्तर की दुसरी बात का निषेध करने के आग्रह में पड़ने वाला अभिनिवेशिक मिथ्यात्वी कहलाता है।
जीर्ण-शीर्ण पुस्तकों को लिपिबद्ध करने में बहुत भले हो जाती हैं इसलिए अक्षर और अंकों का नम्बर लिखने में दृष्टि दोष से यदि दुर्लभ राजा की मृत्यु 1087 में हुई हो उसके लिखने की जगह पर भूल से 1087 के 1077 लिखा गया हो, उसमें 8 का 7 बनना भी संभव हो सकता है। परन्तु श्री जिनेश्वरसूरि जी ने दुर्लभ राजा की सभा में चैत्यवासियों को पराभव किया और संयमियों का विहार खुला कराया तब से वसतिवासी सुविहित खरतर कहलाने लगे- यह उल्लेख संवत् 1139 में बने हुए श्री वीर चरित्र में है, यह रचना नवांगी वृत्तिकार खरतरगच्छीय श्री अभयदेव सूरि जी के सन्तानीय श्री गुणचन्द्रगणि जी ने की है।
अन्य गच्छीय पट्टावलियों में जो बहुत ही अर्वाचीन है उनमें खरतरगच्छ की उत्पत्ति सं. 1204 में होना लिखा है, यह मत सरासर भ्रामक व वास्तविकता से परे है।
सं. 1188 में रचित देवभद्रसूरिकृत पार्श्वनाथ चरित्र की प्रशस्ति में 1170 में लिखित पट्टावली में ‘खरतर विरुद' मिलने का स्पष्ट उल्लेख है।
जैतारण राजस्थान के धर्मनाथ स्वामी के मंदिर में सं. 1171 माघ सुदी पंचमी का सं. 1169, सं. 1174 के अभिलेखों में स्पष्ट लिखा है, 'खरतरगच्छे सुविहिता गणाधीश्वर जिनदत्तसूरि।
भीनासर (बीकानेर) के पाश्र्वनाथ के मंदिर में पाषाण प्रतिमा पर सं. 1181 का लेख अंकित है, उसमें भी ‘खरतरगणाधीश्वर श्री जिनदत्तसूरिभिः' लिखा है।
इस तरह यदि सं. 1209 में ही खरतरगच्छ की उत्पत्ति होती तो सं. 1147, सं. 1169, सं. 1171, सं. 1174, सं. 1181 के शिलालेखों में और सं. 1168 व सं. 1170 के ताड़पत्रीय ग्रन्थों में खरतर विरुद मिलने का उल्लेख कैसे सम्भव होता? बिना पिता के पुत्र कैसे? मुनि जिनविजय (कथाकोष प्रस्तावना), पूर्णचन्द्र नाहर (जैन लेख संग्रह, प्रस्तावना, भाग 3), सुखसम्पतिराज भण्डारी (ओसवाल- जाति का इतिहास), डा.ऋषभचन्द्र (जिनवाणी, जैन संस्कृति और राज., पृष्ठ-256), अगरचन्द जी, भंवरलाल जी नाहटा (खरतरगच्छ का इतिहास), आदि सभी विद्वावनों ने खरतगच्छ की उत्पत्ति वि.सं. 11वीं शताब्दी मानते हैं, तपागच्छीय उपाध्याय धर्मसागर ने जो खरतरगच्छ की उत्पत्ति का काल सं. 1204 लिखा है वह वास्तव में खरतरगच्छ की उत्पत्ति का नहीं है, अपितु सं. 1204 में तो खरतरगच्छ से अन्य शाखा निकली जिसका नाम रूद्रपल्लीय खरतरगच्छ है।
सं. 1305 में रचित युगप्रधानाचार्य गुर्वावली में खरतरगच्छ का उद्भव एवं उसकी परम्परा आचार्य वर्धमानसूरि एवं आचार्य जिनेश्वरसूरि से स्पष्टतः सम्बन्ध जोड़ा है। मुनि जिनविजय ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि ‘प्रभावक चरित्र के वर्णन से यह तो निश्चित ही ज्ञात होता है कि सूराचार्य उस समय चैत्यवासियों के प्रसिद्ध और प्रभावशाली अग्रणी थे। वे पंचाक्षर Tथ चैत्य के मख्य अधिष्ठाता थे। स्वभाव से वे बडे उग्र और वाद-विवाद प्रिय थे। अतः उनका वाद-विवाद में अग्र रूप से भाग लेना असम्भव नहीं, परन्तु प्रासंगिक ही मालूम देता है। शास्त्रकार की दृष्टि से यह तो निश्चित ही है कि जिनेश्वराचार्य का पक्ष सर्वदा सत्यमय था। अतः उनके विपक्ष का उसमें निरूत्तर होना स्वाभाविक ही था। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि राजसभा में चैत्यवासी पक्ष निरूत्तरित होकर जिनेश्वर का पथ राज सम्मानित हुआ और इस प्रकार विपक्ष के नेता का मान-भंग होना अपरिहार्य बना।
इसलिए सम्भव है प्रभावक चरितकार को सूराचार्य के इस मान–भग का उनके चरित्र में कोई उल्लेख करना अच्छा नहीं मालूम दिया हो और उन्होंने इस प्रसंग को उक्त रूप में न आलोकित कर अपना मौन—भाव ही प्रकट किया हो (ओसवाल वंश, पृष्ठ 33-34)।
इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आचार्य जिनेश्वरसूरि तथा सूराचार्य आदि चैत्यवासियों के मध्य अणहिलपुर पत्तन में राजा दुर्लभ की अध्यक्षता में शास्त्रार्थ हुआ था। शास्त्रार्थ-विजय कर जिनेश्वरसूरि ने खरतर विरूद प्राप्त किया था। अतः वे खरतरगच्छ के प्रथम आचार्य/आदि प्रवर्तक हुए। इन्हीं जिनेश्वरसूरि की परम्परा में हुए मुनियों ने चैत्यवासियों के विरुद्ध आंदोलन अनवरत चालू रखा, जो तेरहवीं शताब्दी तक चलता रहा। इस अवधि में अनेक ऐतिहासिक पुरुष एवं घटनाएँ हुईं, जिनसे सुविहित मार्ग विधि पक्ष शुरू किया था, उसे अभयदेव, देवभद्र, वर्धमान, जिनवल्लभ, जिनदत्त, जिनपति, आदि आचार्यों ने पूरा करने का प्रयास किया और उन्हें अपरिमित सफलता प्राप्त हुई।
मुनि जिनविजय का अभिवचन है कि इस प्रसंग से जिनेश्वरसूरि की केवल अणहिलपुर में ही नहीं, गरे गजरात में और उसके आस-पास के मारवाड़, मेवाड, मालवा, बागड, सिंध और दिल्ली तक के प्रदेशों में खूब ख्याति और प्रतिष्ठा बढ़ी। जगह-जगह सैकड़ों श्रावक उनके भक्त और अनुयायी बन गये। अजैन गृहस्थ भी उनके भक्त बनकर नये श्रावक बने। अनेक प्रभावशाली और प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने उनके पास यति मुनि दीक्षा लेकर उनके सुविहित शिष्य कहलाने का गौरव प्राप्त किया। उनकी शिष्य संतति बहुत बढ़ी और वह अनेक शाखा–प्रशाखाओं में फैली। उसमें बड़े-बड़े विद्वान, क्रियानिष्ठ और गुणगरिष्ठ आचार्य, उपाध्यायादि समर्थ साधु पुरुष हुए। चरितादि के रचयिता वर्धमानसूरि, पार्श्वनाथ चरित एवं महावीर चरित के कर्ता गुणचन्द्र गणि अपर नाम देवभद्रसूरि, संघ पट्टकादि अनेक ग्रन्थों के प्रणेता जिनवल्लभसूरि इत्यादि अनेकानेक बड़े-बड़े धुरन्धर विद्वान और शास्त्रकार जो उस समय उत्प हुए और जिनकी साहित्यिक उपासना से जैन वांगमय-भंडार बहुत कुछ समृद्ध और सुप्रतिष्ठित बना- इन्हीं जिनेश्वरसूरि के शिष्य-प्रशिष्यों में थे। (कथाकोष, प्रस्तावना, पृष्ठ 2)
उपसंहार
उल्लेखित अनेकानेक ऐतिहासिक प्रमाणिक प्रमाणों से स्पष्ट है कि आचार्य जिनेश्वरसूरिजी ने अपनी आचार-निष्ठा, प्रखर तेजस्विता, स्पष्टवादिता, प्रखर प्रज्ञा से अणहिलपुर पाटण में वि.सं. 1080 में दुर्लभ राजा के समक्ष चैत्यवासी सूराचार्य की सभी अशास्त्रीय, अकरणीय और अवांछनीय का खण्डन और विध्वंश करके शास्त्रीय, करणीय एवं वांछनीय तत्वों का मण्डन और नवनिर्माण किया। तब से जिनेश्वरसूरि का अनुयायीवर्ग या प्रभावित वर्ग उनके लिए खरतर सम्बोधन व्यवहृत करने लगा। खरतरगच्छ से बहुशाखी वटवृक्ष की सघन छाया में लक्ष-लक्ष/कोटि-कोटि, धर्मप्राण नर-नारियों ने विश्रान्ति की आत्मशान्ति की अनुभूति की और करते रहेंगे।
वि.सं. 2080 में जैन संस्कृति के अभिनव उन्मेष का परिचायक सर्वप्राचीन ‘खरतरगच्छ' सहस्त्रशताब्दि पूर्ण करने जा रहा है। इस अनुपम अवसर पर उच्च, उज्ज्वल, महान खरतरगच्छ के अभ्युदय, विकास और अभिवर्धन में अपनी अहम् भूमिका अदा करें।